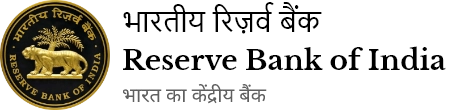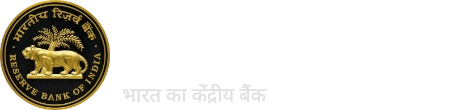i) वार्षिक रिपोर्ट
रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट एक सांविधिक प्रकाशन है जिसे वार्षिक लेखाबंदी के दो महीने के भीतर जारी किया जाता है। यह केंद्रीय बोर्ड द्वारा अर्थव्यवस्था की स्थिति, वर्ष के दौरान बैंक के कामकाज और रिज़र्व बैंक के तुलन- पत्र के संबंध में एक रिपोर्ट है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के आकलन और आगे आने वाली अवधि में इसकी संभावनाओं को भी प्रस्तुत करता है।
ii) भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट
यह बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36(2) के अंतर्गत बैंक का एक सांविधिक वार्षिक प्रकाशन है। यह भारतीय बैंकिंग और गैर-बैंकिंग क्षेत्र के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करते हुए वैश्विक बैंकिंग क्षेत्र की गतिविधियों का अवलोकन प्रदान करता है। आम तौर पर यह रिपोर्ट हर वर्ष नवंबर/दिसंबर में जारी की जाती है।
iii) मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट
यह बैंक का विषय-आधारित वार्षिक प्रकाशन है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित समसामयिक और प्रासंगिक आर्थिक मुद्दों पर व्यापक शोध कार्य उपलब्ध कराता है।
iv) मौद्रिक नीति रिपोर्ट
यह बैंक का छमाही सांविधिक प्रकाशन है, जो सामान्यतः अप्रैल और अक्तूबर में जारी किया जाता है। यह समष्टि आर्थिक संभावना तथा संवृद्धि और मुद्रास्फीति पर पूर्वानुमान प्रदान करता है। इसमें जोखिमों, कीमतों और लागतों का संतुलन, वित्तीय बाजार और चलनिधि की स्थिति और बाहरी वैश्विक वातावरण की गतिविधियों को भी शामिल किया जाता है।
v) वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट
यह एक छमाही रिपोर्ट है जो वैश्विक वित्तीय संकट और उसके दुष्परिणाम अर्थात्, मार्च 2010 के बाद से प्रकाशित की जा रही है। यह भारत की वित्तीय प्रणाली की स्थिरता का आकलन; जोखिमों की प्रकृति, गंभीरता और प्रभावों की समीक्षा; तनाव परीक्षण और आघात सहनीयता के परिणाम प्रदान करता है; पूर्वक्रीत नीति प्रतिक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण संकेत प्रदान करता है और वित्तीय क्षेत्र के विकास और विनियमन की पद्धतियों का उल्लेख करता है।
vi) भुगतान प्रणाली रिपोर्ट
यह रिपोर्ट भारत में भुगतान प्रणालियों का अवलोकन प्रदान करती है, जिसमें इसका विधिक आधार, भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड (बीपीएसएस) की भूमिका और कार्य शामिल हैं। इस रिपोर्ट में वर्तमान भुगतान प्रणाली परिदृश्य और इसके आँकड़ों पर भी चर्चा की जाती है। यह रिपोर्ट भारतीय भुगतान प्रणालियों से संबंधित प्रमुख विनियामक गतिविधियों पर भी प्रकाश डालती है। यूपीआई और इसके संवर्धन के लिए एक विशेष खंड प्रदान किया गया है, जहाँ यूपीआई पी2पी और पी2एम सहित यूपीआई लेनदेन में वृद्धि के साथ-साथ यूपीआई लाइट, यूपीआई आईपीओ आदि जैसे यूपीआई से संबंधित अन्य उत्पादों पर विस्तार से चर्चा की जाती है। रिपोर्ट में विभिन्न भुगतान प्रणालियों के लेनदेन की मात्रा और मूल्य, सीमापारीय भुगतान और भारत से आवक-जावक विप्रेषण के पिछले पाँच वर्षों के रुझान पर भी चर्चा की जाती है। इस रिपोर्ट में भुगतान प्रणालियों से संबंधित प्रमुख वैश्विक रुझान भी उपलब्ध करवाए जाते हैं।
vii) राज्य वित्त: बजट का एक अध्ययन
भारतीय रिज़र्व बैंक का वार्षिक प्रकाशन "राज्य वित्त: बजट का अध्ययन" सभी राज्य सरकारों और विधानसभा वाले संघ शासित प्रदेशों की राजकोषीय स्थिति का आकलन प्रस्तुत करता है। प्रत्येक संस्करण में एक समर्पित विषयगत अध्याय होता है जो राज्य वित्त में समकालीन मुद्दे की जांच करता है। इस अध्ययन में राज्यों के बजट दस्तावेजों से संकलित व्यापक डेटासेट शामिल होता है। इस अध्ययन के साथ-साथ आरबीआई की वेबसाइट पर ई-स्टेट्स डेटाबेस भी जारी किया जाता है, जो 1990-91 से लेकर अब तक स्प्रेडशीट प्रारूप में राज्यों के वित्त पर समय-शृंखला डेटा प्रदान करता है।
viii) नगर निगम वित्त संबंधी रिपोर्ट
नीति और अनुसंधान के लिए उच्च गुणवत्ता वाले डेटा प्रदान करने की आरबीआई की प्रतिबद्धता के के भाग के रूप में, आरबीआई ने 2022 में स्थानीय निकायों के वित्त पर विषयगत द्विवार्षिक रिपोर्ट शुरू की। यह रिपोर्ट भारत में 90 प्रतिशत से अधिक नगर निगमों के बजटीय डेटा को संकलित और विश्लेषित करती है, जिससे शहरी स्थानीय निकायों की राजकोषीय स्थिति का गहन विश्लेषण मिलता है।
ix) पंचायती राज संस्थाओं का वित्त
यह द्विवार्षिक रिपोर्ट लगभग 2.6 लाख ग्राम पंचायतों के वित्त का पहला व्यापक, अखिल भारतीय मूल्यांकन प्रदान करके स्थानीय निकाय संबंधी डेटा की उपलब्धता को काफी आगे बढ़ाती है। पंचायती राज संस्थाओं के वित्त का राज्य-स्तरीय विश्लेषण प्रस्तुत करके, यह रिपोर्ट भारत में ग्रामीण स्थानीय निकायों पर लंबे समय से चली आ रही डेटा संबंधी कमी को दूर करती है।
x) भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन और इसका साप्ताहिक सांख्यिकीय अनुपूरक
मासिक आधार पर प्रकाशित होने वाले भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन में शीर्ष प्रबंधन के भाषण, आलेख और प्रमुख वर्तमान सांख्यिकी शामिल होते हैं। बुलेटिन में प्रकाशित अर्थव्यवस्था की स्थिति आलेख में शोध कर्मचारियों के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने वाले विश्लेषणात्मक आलेख के अलावा अर्थव्यवस्था की व्यापक मासिक समीक्षा भी शामिल होती हैं। वर्तमान सांख्यिकी खंड प्रमुख संकेतकों पर डेटा प्रदान करता है, जिसमें वित्तीय बाजार, मुद्रा और बैंकिंग, कीमतें, सरकारी लेखा और खजाना बिल, बाह्य क्षेत्र और भुगतान प्रणाली संकेतक शामिल हैं।
मौद्रिक नीति वक्तव्य और बैंक द्वारा जारी की जाने वाली प्रमुख रिपोर्टें, जैसे, वार्षिक रिपोर्ट, भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट और वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट इस मासिक प्रकाशन के पूरक के रूप में जारी की जाती हैं। बुलेटिन के भाग के रूप में मौद्रिक नीति रिपोर्ट भी प्रकाशित की जाती है।
मासिक आरबीआई बुलेटिन का साप्ताहिक सांख्यिकीय संपूरक (डब्ल्यूएसएस) एक उच्च आवृत्ति वाला डेटा प्रसार स्रोत है और यह आरबीआई के तुलन-पत्र, आरक्षित निधि की स्थिति, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का समेकित तुलन-पत्र, मौद्रिक और वित्तीय बाजार संकेतक और सरकार के बाजार उधार संबंधी सूचना प्रकाशित करता है। आमतौर पर यह दस्तावेज़ प्रत्येक शुक्रवार की शाम को जारी किया जाता है।